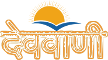दल और सरकार
दमा.गो.वैद्य
भारतीय जनसंघ की स्थापना की अद्र्र्धशताब्दी पूर्ण होने के अवसर पर, गत 21 अक्तूबर को दिल्ली के तालकटोरा मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था।
इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा ने जनसंघ के साथ अपने अटूट रिश्ते का अहसास जताकर निस्संदेह अच्छा कार्य किया है। पुरातन का नवीनता से नाता इसी प्रकार तो जोड़ा जाता है। अतीत का स्मरण और उससे सम्बंध शक्तिदायक होता है, यही हमारे देश की परम्परा का गुण है।
दल क्यों जरूरी है?
सुना है कि इक्कीस अक्तूबर के इस कार्यक्रम में गड़बड़ी हो गई। कही-सुनी और समाचार पत्रों में पढ़े समाचार के अनुसार प्रधानमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम में देर से पहुंचे और वे समझ बैठे थे कि उन्हें दल की ओर से उचित सूचना नहीं मिली थी। किन्तु बाद में उन्होंने ही स्पष्ट किया कि इसमें दल की कोई गलती नहीं थी। उनके सचिवालय (पीएमओ) की ओर से ही उन्हें ठीक जानकारी नहीं मिली थी। उनके इस स्पष्टीकरण के मिलने तक तो पत्रकारों ने बात का बतंगड़ बना दिया। बताया गया कि श्री आडवाणी ने भी अपने भाषण में कहा कि दल को विरोधी दल की भूमिका ग्रहण करते हुए सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए। ये दोनों नेता तो जनसंघ से लेकर भाजपा तक के इतिहास के सजग पुरोधा रहे हैं और उनके महत्व, उनके विचारों के औचित्य को कौन नकारेगा?
सवाल उठता है कि दल और सरकार के बीच कोई अंतर होना चाहिए या नहीं? सरकार के निर्णयों पर दल में चर्चा होनी चाहिए या नहीं? चर्चा करनी न हो या अंतर को समाप्त कर देना हो तो फिर संगठन की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी? अनेक राजनीतिक दलों ने इस अंतर को समाप्त कर दिया है, फिर भी प्रश्न तो रहता ही है कि दल या संगठन का सरकार से कैसा रिश्ता हो? हमने संसदीय प्रजातांत्रिक पद्धति को अपनाया है, जिसमें एक से ज्यादा दलों का होना अनिवार्य है। प्रजातंत्र होने के कारण चुनाव अपरिहार्य हैं और चुनकर आए प्रतिनिधियों का दल बनना भी उतना ही आवश्यक है। अब राजनीतिक दल होने के कारण उसका ध्येय सत्ता-प्राप्ति होना स्वाभाविक ही है। सामान्यत: सत्ता में आने तक, संगठन और विधायक दल में कोई मतभेद होना या टकराव होना संभव नहीं होता, सत्तारूढ़ होने के बाद ही टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है।
और परम्परा भी
इग्लैण्ड में 1945 में लेबर पार्टी सत्ताधीश हुई और क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। बताया जाता है कि ओ हेराल्ड लास्की उस समय लेबर पार्टी के अध्यक्ष थे। इन दोनों की पटरी नहीं बैठी और लास्की को जाना पड़ा। आज भी वही स्थिति जारी है। टोनी ब्लेयर में दोनों पदों की एकत्रीकरण हुआ जान पड़ता है। जब ब्लेयर सांसद थे, उस समय संसदीय दल और दल का नेतृत्व उनके पास ही था।
हमारे देश में भी लगभग ऐसी ही स्थिति रही है। पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस समय पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। उनमें भी मतभेद हुआ और टंडन को जाना पड़ा और दल की धुरी भी नेहरू ने संभाली। पं. नेहरू बड़े कुशल और पुराने जमाने के कार्यकर्ता थे, उनमें इन दोनों जिम्मेदारियों को वहन करने की प्रतिभा नहीं थी, यह कौन कहेगा! फिर भी उन्होंने दल की अध्यक्षता तो छोड़ी परन्तु दल का अध्यक्ष नियुक्त करते समय इतनी सावधानी अवश्य बरती कि आने वाला अध्यक्ष कम शक्ति वाला हो। उत्छंगराय ढेबर, संजीव रेड्डी, संजीवैया ये सब पं. नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल के पार्टी अध्यक्ष रहे। उनके अंतिम काल में कामराज दलीय अध्यक्ष थे।
श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं उस समय कामराज पार्टी अध्यक्ष थे। उन दोनों की नहीं पटी तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को ही तोड़ डाला। इससे तो यही सिद्ध हुआ कि संसदीय दल ही श्रेष्ठ होता है। कामराज की भी छुट्टी हुई और उसके बाद देवकांत बरूआ, देवराज अर्स, शंकरदयाल शर्मा जैसे इंदिरानिष्ठों ने ही पार्टी अध्यक्ष पद विभूषित किया। बाद में इस नौटंकी से ऊबकर स्वयं श्रीमती गांधी ने दल की अध्यक्षता भी अपने पास रख ली। यही परम्परा उनके पुत्र राजीव ने आगे चलाई और फिर नरसिंह राव ने भी वही राग अलापा। आज सोनिया भी वही कर रही हैं, फर्क इतना ही है कि वे प्रधानमंत्री नहीं बन पाईं, यदि बन जातीं तो पार्टी की अध्यक्षता तो छोड़ती नहीं। जब वे कांग्रेसाध्यक्षा बनीं तो उस समय सांसद भी नहीं थीं फिर भी संसदीय दल की अध्यक्षता उन्होंने अपने पास रखी थी।
संघ का विचार
सौभाग्यवश भाजपा अभी तक इस बिन्दु तक पहुंची नहीं है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा के नेतागण भी यह मानते हैं कि संसदीय प्रजातांत्रिक प्रणाली में संसदीय दल का यानी उनके नेताओं का वर्चस्व रहना अपरिहार्य है। श्री आडवाणी ने जब यह कहा कि पार्टी को सरकार विरोधी रवैया नहीं अपनाना चाहिए, तब उसका अर्थ तो संभवत: इसी वर्चस्व की पुष्टि करता है। दल और सरकार के बीच विरोध आम जनता के बीच न आए, यह तो समझा जा सकता है, और ठीक भी है परन्तु पार्टी को सरकार की नीतियों, निर्णयों की जानकारी होनी चाहिए, उसके औचित्य अथवा अनौचित्य पर चर्चा होनी चाहिए तथा पार्टी का भी कोई मत हो सकता है। इन सब बातों को महत्वहीन या गौण तो नहीं माना जा सकता। यदि दल के मत का महत्व है तो उसे प्रकट करने की पद्धति दिशा और तौर-तरीके क्या होने चाहिए? कुछ समय पूर्व जब श्री कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा के अध्यक्ष थे, उस समय सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश को स्थान देने सम्बंधी निर्णय लिया था। पत्रकारों ने जब श्री ठाकरे से इस सम्बंध में पूछा तो उन्होंने अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की। क्या यह स्थिति ठीक है?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इस बारे में कोई चर्चा कभी भी नहीं हुई और चर्चा का प्रयोजन ही नहीं है। संघ का राजनीति में तो दखल नहीं है, पर उसके कुछ स्वयंसेवक राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत अवश्य हैं। इतने वर्षों का संगठनात्मक अनुभव संघ के पास है ही, इस कारण संघ का यह स्पष्ट मानना है कि संगठन चाहे सत्तारूढ़ हो या न हो, उसकी प्रतिष्ठा तो रखी जानी चाहिए, उसकी श्रेष्ठता पर भी कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। दल अर्थात् संगठन के कार्यकर्ता, संसदीय गुट के पिछलग्गू नहीं बने रहें। सरकार को यदि आनंद हो तो दल भी अपनी पूंछ हिलाए और सरकार को कोई डर हो तो उसकी लुका-छिपी हो ऐसा दल बेकार साबित होगा। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को इसी स्थिति में ला दिया था। इसीलिए वह दल ही आज समाप्त प्राय: हो गया है। भाजपा भी ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहती है, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि आज उसकी पहचान "पार्टी विद ए डिफरेन्स' जैसी है। भाजपा की कार्यवाही भी इसी दावे की पुष्टि करने वाली होनी चाहिए।
महज प्रतिष्ठा के लिए
दल, पार्टी या संगठन इसकी प्रतिष्ठा को सदा ऊंचा टिकाए रखने के लिए कुछ बातें बहुत आवश्यक हैं। उनमें से एक तो यह कि पार्टी के प्रत्येक स्तर पर ऐसे कार्यकर्ता हों, जिन्हें सरकारी पद प्राप्त करने हेतु चुनाव लड़ने की कोई महत्त्वाकांक्षा न हो, और न कोई सरकारी पद पर बैठने की लालसा ही हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक प.पू. श्री गुरुजी ने एक बार बातचीत के दौरान कहा था कि पं. नेहरू या सरदार पटेल में से कोई भी एक सरकार में न रहते हुए पार्टी में रहा होता तो कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा नहीं हुई होती। तात्पर्य यही कि जिन व्यक्तियों को सत्ता में या सरकार में जाने का मोह न हो, ऐसे कुछ लोगों को तो पार्टी के उच्च स्थान पर रहना चाहिए। कम से कम अध्यक्ष, सचिव जैसे महत्त्वपूर्ण पदों पर आसीन कार्यकर्ताओं को सत्ता के सरकारी पदों पर बैठने की लालसा नहीं होनी चाहिए। कइयों को यह भ्रम है कि सत्ता की लालसा से ही लोग राजनीति में प्रवेश करते हैं। जिन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की थोड़ी भी जानकारी है, वे ऐसे भ्रम में कभी नहीं रहेंगे। संघ में अनेक प्रचारक हैं, आखिर किसलिए वे अपने जीवन की आहुति देते हैं? उन्हें अपने लिए किस लाभ की अपेक्षा होती है? प्रचारकों के अतिरिक्त और भी ऐसे अनेक लोग अपना सारा समय संघ के लिए देते हैं तो उन्हें किस स्वार्थ की प्राप्ति होती है? राष्ट्रीय जीवन में राजनीति का महत्व तो वे जानते ही हैं। यह राजनीति राष्ट्र के लिए हितकारी हो, जनकल्याण के लिए उत्सुक हो, देश की समृद्धि के लिए प्रत्यनशील हो यही उनकी मान्यता होती है। यदि संघ में ऐसे कार्यकर्ता हो सकते हैं तो भाजपा में क्यों नहीं? भाजपा में भी ऐसे विचार के लोग हों और संगठन के सूत्र भी ऐसे लोगों के पास हों तो दल भी ठीक चलेगा और सत्ता मिलने पर सत्ताधारी भी ठीक काम करेंगे। तलपट
विश्व का सबसे लम्बा पत्र जो श्रीराम के नाम लिखा गया है, में कुल 1 करोड़, 11 लाख, 11 हजार 111 अक्षर है। अक्षर भी सिर्फ "राम', "राम' शब्द हैं। यह पत्र मालेर कोटला (पंजाब) निवासी श्री चरण सिंह गुप्ता ने श्रीराम चंद्र जी को अयोध्या के पते पर लिखा (टंकित किया) है। यह पत्र 66न्35 सेंटीमीटर आकार की कागज के 3865 पृष्ठों पर लिखा गया है। जिसका कुल वजन 41 किलो बनता है। यदि सभी "राम' शब्द एक पंक्ति में लगा दिए जाएं तो उनसे 125 किमी लम्बी पंक्ति बन जाएगी और यदि सभी कागज एक-एक करके लम्बवत् रखे जाएं, तो 2.21 कि.मी. 35 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी बन जाएगी। इस पत्र को लिखने में तीन वर्ष का समय लगा है।